किसी भी राष्ट्र की उन्नति का पथ वहाँ प्रदान की जाने वाली बेसिक शिक्षा की स्थिति पर निर्भर करता है। बेसिक शिक्षा का स्तर ही यह तय करता है कि वहां की उच्चतर शिक्षा कैसी होगी? केवल भौतिक संरचनात्मक सुविधाएं ही शैक्षिक स्तर को निर्धारित नहीं करतीं अपितु शिक्षार्थी, शिक्षक, समुदाय व शासन-प्रशासन का बेहतर समन्वयन ही उसे गौरवशाली स्थान दिला सकता है। राष्ट्र की बेसिक शिक्षा की समस्याओं का विश्लेषण कर सम्यक् समाधान प्रस्तुत करती पुस्तक ‘शिक्षा के पथ पर’ इन दिनों बेसिक शिक्षा जगत् में खासी चर्चा में है। यह कृति न केवल बेसिक शिक्षकों अपितु शिक्षार्थियों, अभिभावकों, प्रशिक्षकों एवं बेसिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न अधिकारियों के लिए भी एक मार्गदर्शिका है। 134 पृष्ठों की यह पुस्तक कुल 21 अध्यायों में बेसिक शिक्षा की सम्यक् तस्वीर प्रस्तुत करती है।

प्रथम अध्याय में भाषा की कक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अवसर की विस्तृत चर्चा की गई है। कक्षा-कक्ष में बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर मिलें, इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय आनंदघर के रूप में विकसित हों। इससे बच्चे बिना डर, संकोच व लज्जा के शिक्षकों से रूबरू हो अधिकतम सीख सकेंगे। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को गति देते हैं समूह गीत। स्थानीय परिवेश से संबंधित गीतों द्वारा बच्चों का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जुड़ाव सहज हो जाता है। तीसरे अध्याय ‘और ताला खुल गया’ में यह बताया गया है कि बच्चों और बड़ों के मनोविज्ञान को परख कर किसी समस्या की जड़ तक कैसे पहुंच जाता है? जबरन बंद किए गए विद्यालय के ताले को खुलवा देना वह भी बिना बल प्रयोग कराये, अपने आप में संप्रेषण-कला का उत्कृष्ट नमूना है।
चौथे अध्याय ‘बाल संसद के रास्ते’ में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाल संसद का गठन कर हुए सुखद बदलाव की चर्चा की गई है। अवसर मिलने पर बच्चों की कल्पनाएं साकार रूप लेने लगतीं हैं। पांचवें अध्याय ‘बदलाव की आधार भूमि बनती दीवार पत्रिका’ में दिखाया गया है कि बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने में किस प्रकार दीवार पत्रिका सहायक सिद्ध हो रही है।
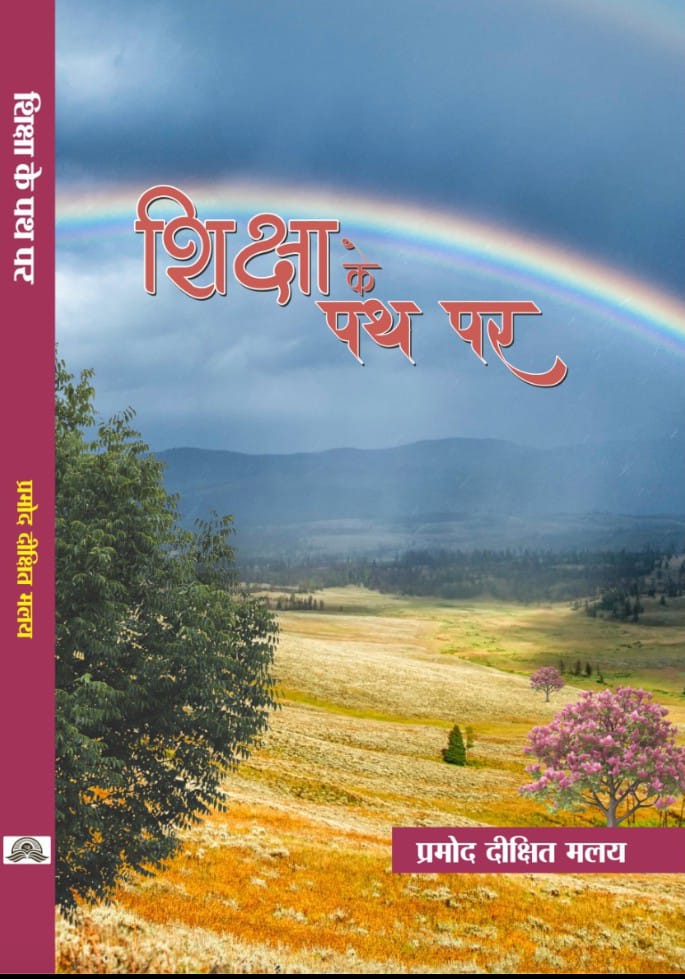
छठें अध्याय ‘शैक्षिक संसाधन और गुणवत्ता : कुछ जरूरी प्रश्न’ में यह दर्शाया गया है कि यदि शिक्षक, अभिभावक और बच्चे सभी मिलकर गुणवत्ता संवर्धन हेतु पूर्ण मनोयोग से कार्य करें तो संसाधन आड़े नहीं आते। सातवें अध्याय ‘विज्ञान की कक्षा में एक दिन’ में बड़े ही रोचक ढंग से बच्चों को सरल मशीन के बारे में बताया गया है। मजे की बात है कि बच्चे स्वयं मशीन के बारे में अपनी समझ बनाते दिखे। आठवें अध्याय ‘रोचक गतिविधियों द्वारा भाषा शिक्षण : एक प्रयोग’ में बहुत ही रोचक ढंग से विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्दों की गतिविधि बच्चों के बीच कराई गई है। तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के बीच किया गया यह प्रयोग बहुत ही प्रेरणाप्रद रहा और बच्चे खेल-खेल में सीखने लगे। नवें अध्याय ‘शिक्षक बनने में किताबों की भूमिका : मेरे अनुभव’ के द्वारा लेखक ने बेबाकी से स्वीकार किया है कि किस प्रकार दिवास्वप्न, बाल संसद, दीवार पत्रिका, समरहिल आदि पुस्तकों ने उनके व्यक्तित्व को निखारने में मदद की। दसवें अध्याय- उसे कुछ नहीं आता (कविताएं) में कतिपय कविताओं यथा उसे कुछ नहीं आता, सुनो शिक्षको, सुबह की घंटी, शाम की घंटी, बच्चे एवं होमवर्क के माध्यम से यह बताया गया है कि बच्चे बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। बच्चों की तुलना खाली घड़े या कोरी स्लेट से कतई नहीं की जा सकती।
11वें अध्याय ‘दिवास्वप्न के आलोक में वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य’ में ‘दिवास्वप्न’ के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन को आनंददायक बनाने की चर्चा की गई है। 12वें अध्याय ‘बच्चों की रचनात्मकता में बाधक होमवर्क’ के माध्यम से विद्यालय में दिए जाने वाले गृहकार्य (होमवर्क) के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया गया है। लेखक की राय में होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। अगर दिया जाए तो वह छात्रों की रुचि के अनुकूल हो। 13वें अध्याय ‘ज्ञान सर्जना का मुक्त प्राकृतिक मंच है शैक्षिक भ्रमण’ के माध्यम से लेखक ने स्वानुभूत पलों को याद करते हुए शैक्षिक भ्रमण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला है और बताया है कि नवल ज्ञान की सर्जना में शैक्षिक भ्रमण किस प्रकार सहायक होते हैं। 14वें अध्याय ‘प्राथमिक शिक्षा में विज्ञान शिक्षण की चुनौती भरी राह’ में विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों की चर्चा की गई है तथा विज्ञान के प्रोफेसर-डॉक्टर, शिक्षकों आदि द्वारा किए जाने वाले अंधविश्वासों पर कटाक्ष किया गया है। 15वें अध्याय ‘कक्षा में बच्चों से बातचीत’ के अंतर्गत बातचीत के माध्यम से बच्चों को कक्षा-कक्ष में अभिव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर दिए जाने पर जोर दिया गया है। निश्चित रूप से यह तरीका संवेदनशील मुद्दों पर बच्चों की राय जानने का बहुत प्रेरक एवं सराहनीय ढंग है।
16वें अध्याय ‘महिला शिक्षा : अतीत से वर्तमान तक’ में महिला शिक्षा के संदर्भ में सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए प्रयासों की चर्चा की गई है। वस्तुत: शिक्षित स्त्री ही सुशिक्षित समाज का निर्माण कर सकती है। 17वें अध्याय ‘पढ़ने की संस्कृति पर स्कूली शिक्षा का दबाव’ में इस बात पर चर्चा की गई है कि पढ़ाना केवल स्कूली शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों में छपी सामग्री के वाचन तक सीमित नहीं है बल्कि यह अपने अस्तित्व की पहचान है। 18वें अध्याय ‘गिजुभाई बधेका : शैक्षिक प्रयोग का धनी व्यक्तित्व’ में बताया गया है कि लगभग 100 वर्ष पूर्व जिस प्रकार गिरजाशंकर भगवान जी बधेका (गिजुभाई बधेका) ने तत्कालीन बुनियादी शिक्षा को आनंदमय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सार्थक प्रयोग किये, उनकी प्रासंगिकता आज भी देखी जा सकती है। 19वें अध्याय ‘उम्मीद जगाते शिक्षकों के सम्मान का दिन’ -विश्व शिक्षक दिवस (5 अक्टूबर) को संदर्भित यह आलेख वर्तमान समय में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिक्षकों को समर्पित है।
ऐसे सम्मान से अन्य शिक्षकों में भी नवल ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। 20वें अध्याय ‘बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जगाता मीना मंच’ के अंतर्गत बालिकाओं में शिक्षा की प्रति रुचि जगाने के निमित्त मीना मंच की सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है। इससे बालिकाओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं पहल करने की सोच में निखार आता है। आखिरी अध्याय ‘बच्चों की रचनात्मकता को दिशा देती दीवार पत्रिका’ के अंतर्गत दीवार पत्रिका क्या है? इसके निर्माण में आने वाली चुनौतियों एवं सावधानियों की चर्चा की गई है इस लेख में। वास्तव में दीवार पत्रिका शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन करने को प्रेरित करती है।
पुस्तक ‘शिक्षा के पथ पर’ पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कक्षा कक्ष की प्रत्येक गतिविधि आँखों के सम्मुख घटित हो रही है। पाठक स्वयं उन चुनौतियों से गुजरते हुए उनके संभावित समाधान की परिकल्पना करने लगता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह पुस्तक बेसिक शिक्षा विभाग की अधुनातन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक शिक्षा जगत में समादृत होगी, ऐसा विश्वास है।






